जब तुम नहीं थीं, तब मैं तुम्हारा होना चाहता था. एक साया सा दाखिल होता था ख्यालों में. उसका कोई चेहरा नहीं होता था. लेकिन उस अनजाने साये से लिपटकर मैं खूब रोता था और मां के पूछने पर कि क्यों आंखें सूजी हैं मैं हमेशा कहता कि देर रात तक पढ़ता रहा. मां की पहरेदारी में अपने कहे को सच साबित करने के लिए मैं सचमुच कोई किताब खोलकर बैठा या अधलेटा सा रहता. मां आश्वस्त हो जाती लेकिन पापा नहीं. उन्हें अपने बेटे के झूठ समझ में आते थे. लेकिन उन्होंने चुप्पियों में ही अपना जीवन साधना सीखा था. मां के दिन भर बड़बड़ाने को वो अपने मौन से ऐसे उठाकर किनारे रख देते जैसे कोई पढ़ा हुआ अखबार रख देता है. पिता के लिए मां पढ़ा हुआ अखबार थीं या अनचीन्हा अक्षर, यह मैं उनसे कभी पूछ ही नहीं पाया. वो हर काम बड़ी मुस्तैदी से करते थे और चुपचाप. मेरे फिसड्डी नतीजों के बावजूद उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा. बहन की शादी करने के बाद वो मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही देखने लगे थे.
उनकी खामोश निगाहों का सामना करने की ताकत मुझमें नहीं थी. तब तक तुम मेरी जिंदगी में आ ही चुकी थीं. तुम्हें तो मालूम है ना? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होगा, क्योंकि तुम्हारा न कोई नाम था, न चेहरा. तुम बस एक साया थीं. मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थीं. मेरी तुम थीं. तुम जिसे मैंने अपने कल्पनालोक में गढ़ा था. मैं पढ़ाई में फिसड्डी सही लेकिन प्रेम में फिसड्डी नहीं रहना चाहता था. सो मैंने ढेर सारी कहानियां तुम्हारी और अपनी गढ़ डालीं. दोस्तों को जब वो कहानियां सुनाता तो वे ईष्र्या से जलभुन जाते. धीरे-धीरे वो कहानियां तुम तक भी जा पहुंची. तुम्हारी किसी सहेली ने मुझे बताया था कि कैसे तुम मेरी कहानी सुनकर रो पड़ी थीं. कितनी देर तक रोती रहीं. और किसी पुराने एलपी की तरह बार-बार उससे वो कहानी सुनती रहीं. उस रोज पहली बार मुझे लगा कि वो तुम ही हो जो रोज साया बनकर मेरे सिरहाने बैठती हो कभी हाथ पकड़कर घूमती हो मेरे साथ.
मैं अब तक तुम्हारा नाम नहीं जानता था. चेहरा भी नहीं. बस मेरी झूठी कहानियां ही वो पुल थीं, जिसके उस पार तुम थीं. मैंने और तेजी से कहानियां लिखना शुरू किया. मेरी कहानियों में दर्द के धारे बहते थे. लोग आह आह करते थे. और मैं किसी खिलाड़ी की तरह खुश होता था अपनी जीत पर. कहानियों के चक्कर में मेरे इम्तिहानों के नतीजे और खराब होने लगे और मैं फेल हो गया. मुझे पहला ख्याल आया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी. पहली बार फेल होने पर पापा का चेहरा सामने नहीं आया. सारा दिन मैं मुंह छुपाये बैठा रहा. लेकिन शाम मेरे लिए एक सुंदर पैगाम लेकर आई थी. जानती हो वो सुंदर पैगाम क्या था.
नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा कि वो सुंदर पैगाम क्या था. वो पैगाम यह था कि तुम भी फेल हो गई थीं. मैं अपने पास होने पर कभी इतना खुश नहीं हुआ, जितना तुम्हारे फेल होने पर हुआ. सचमुच. अब तक मैं तुम्हारा नाम जान गया था. पुष्पा. यही नाम था न तुम्हारा.
सच कहूं मुझे तुम्हारा नाम कभी अच्छा नहीं लगा. किसी पुराने जमाने की हीरोईन जैसा नाम. मैं तो डॉली, मोना, नैन्सी जैसे मॉर्डन नाम की कल्पना करता था या फिर रितु, अरुणिमा, कशिश, रिद्मा जैसे मनोहारी नामों की कल्पना करता था. वैसे मुझे कौन सा अपना ही नाम अच्छा लगता था. मनोज. भला कोई नाम है. एक क्लास में पांच मनोज तो हमेशा से रहे. मुझे पापा पर इस बात का गुस्सा भी हमेशा रहा कि वो अपने बेटे का एक कायदे का नाम नहीं रख सके. ऐसे लोगों को मां-बाप बनने का हक ही नहीं होना चाहिए जो बच्चों का कम से कम एक अच्छा सा नाम न रख सकें. बहरहाल, मेरे मनोज और तुम्हारे पुष्पा होने को अब कोई बदल नहीं सकता था.
उस रात मैं कितना खुश होकर सोया था कि जिसकी याद में न पढ़कर मैं फेल हुआ वो भी फेल हो गई. जरूर उसने भी मेरे सपने देखने में रातें गारत की होंगी और नतीजा मेरे बराबर आ पहुंचा. असल में यह हमारे प्रेम का नतीजा था जो फेल होने के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहा था. इस तरह एक साथ बीए में फेलकर हमने अपने प्रेम का पहला इम्तिहान पास किया. लेकिन पापा, वो अब चुप रहने वाले कहां थे. वो अंदर ही अंदर मुझसे बदला लेने या मुझे दुरुस्त करने की योजनाएं बनाने में लगे थे. मेरा उनका सामना अब और कम होने लगा था.
मैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता था. मैं जमकर कहानियां लिखता था. इस बीच मेरी कहानियों की ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी. कुछ कहानियां छपने भी लगीं. मेरी उत्सुकता अब सिर्फ मेरी कहानी पर तुम्हारी प्रतिक्रिया जानने की रहती थी. मैं हर उस व्यक्ति से बात करता, जो तुम्हें जानता था ताकि शायद कभी बात निकले कि तुमने मेरी कहानी के बारे में कुछ कहा. उधर तुम्हारी सहेली जो हमारे बीच संवाद का इकलौता पुल थी शादी करके दूसरे शहर जा चुकी थी. दोस्तों के सामने इतनी डींगे मार चुका था अपने और तुम्हारे बारे में कि उनसे किस मुंह से कहता कि मेरी एक मुलाकात तो करवा दें. उस दिन मां ने मेरे लिए निर्जला व्रत रखा था. मां ने कहा शाम को घर जल्दी आ जाना पूजा में तेरा होना जरूरी है. मैं मां के पांव छूकर निकला. पापा सामने पड़े लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया. तभी एक दोस्त ने बताया कि आज के अखबार में तेरी कहानी छपी है और फोटो भी. मनोज कुमार अब फिल्मी मनोज कुमार टाइप हीरो हो चले थे. सारा दिन कॉलेज में कॉलर उठाये घूमता रहा. क्लास की उन लड़कियों को भी भाव नहीं देता था जो मेरी कहानियों पर फिदा थीं क्योंकि मैं तो तुम पर फिदा था. उस रोज तुम्हारी किसी सहेली ने मुझे संदेश दिया कि तुमने मेरी कहानी पर बधाई दी है और तुम मुझसे मिलना चाहती हो. शाम आठ बजे का वक्त हमारी मुलाकात का तय हुआ. मैं कितना खुश था बता नहीं सकता. बिल्कुल आम सी पे्रम कहानी जो हमारे बीच अब घटने वाली थी उसको लेकर कितना खास उत्साह था. फिल्मों में देखे सारे मिलन के दृश्य याद आने लगे. कि तुम मेरा हाथ थामोगी फिर शरमा जाओगी. वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था. कट ही नहीं रहा था. सेंकेंड की सुइयों पर नजर टिकी हुई थी. इस बीच मां के व्रत वाली बात दिमाग से ही निकल गई थी.हमारा लीला टाकीज के पास वाले शहर के सबसे कम चलने वाले रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था. मैं वहां समय से पहले तैनात था. अपनी बेसब्री को अपने भीतर निगलते हुए एक किताब में नजरें गड़ाये था. एक खुली पेन जो मेरी किताब के प्रति गहनता को सिद्ध करे को बेवजह इधर-उधर किताब पर टहला रहा था. इसी बीच मेरा एक दोस्त आ पहुंचा.
पापा को दिल का दौरा पड़ा था. मुझे ऐसे हालात का सामना करना आता ही नहीं था. मैं सदा से निकम्मा रहा. घर पहुंचा तो पता चला कि सब अस्पताल गये हैं. अस्पताल पहुंचा तो पापा के सामने खड़े होते ही टांगे थर थर कांपने लगीं. जैसे मैं अपनी जिंदगी के सारे इम्तिहानों के रिजल्ट लेकर सामने खड़ा हूं. पापा की आंखे मेरे चेहरे पर थीं. मैं अरसे बाद उन आंखों में आंखें डालकर खड़ा था कि पापा शायद आंखों से कुछ कहना चाहते हैं, तभी मां की रोने की तेज आवाज ने मुझे चौंकाया. मां के रोने पर मुझे ख्याल आया कि उसका निर्जल व्रत है जो उसने मेरे लिए रखा है. पापा की आंखें अब भी खुली थीं. लेकिन पापा जा चुके थे. पहली बार जब मैंने पापा की आंखों में देखा तो वे मरी हुई आंखें थीं. किसी की आंखों में जीने के तमाम ख्वाब देखना और किसी की चाहत में मर जाने की बातें कहानी में लिखने वाला कहानीकार असल जिंदगी में अपने मृत पिता की आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था.
पापा को पता था कि उनका बेटा नाकारा है. कभी कुछ नहीं कर पायेगा. इस बात का अहसास मुझे उनकी नौकरी की जगह नौकरी के लिए अप्लीकेशन लिखते समय हुआ. उस दिन मैं इतना रोया, इतना रोया कि मेरी तमाम कहानियां उसमें जरूर बह गई होतीं अगर उन्हें पढऩे वालों ने संभाल न रखा होता. रिटायरमेंट से ठीक कुछ महीने पहले पापा का जाना जैसा उनकी सोची समझी योजना थी. अपने कंधों पर अपना बोझ तबसे लिए घूम रहा हूं. लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाया कि मैं उस दिन तुमसे मिलने क्यों नहीं आ पाया था.
तुम्हारी शादी की खबर मिली थी मुझे. लेकिन अपनी शादी की खबर को मैं अब तक पचा नहीं पा रहा था. पापा जाते-जाते मेरी शादी भी तय कर गये थे. पापा की अंतिम इच्छा के आगे मेरी सारी कहानियां बौनी थीं. मैंने मां की सूनी आंखों में अपनी स्वीकृति रखकर उनके होठों पर एक सूखी मुस्कान जुटाने का उपक्रम किया.
जिस दिन तुम्हारी शादी हुई उस दिन मैंने पहली बार शराब पी. किताबों में पढ़ा, फिल्मों में देखा इस तरह भी असर करता है शायद. यूं मुझे सचमुच इतनी तकलीफ हुई भी थी कि नहीं, इस बारे में मैं पक्की तरह से कुछ नहीं कह सकता लेकिन मेरे मन में यह बात जरूर उठी थी कि मेरी प्रेमिका की शादी हो रही है और मैं शराब भी नहीं पी रहा हूं. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो दुनिया के तमाम प्रेमी मुझे लानतें भेजेंगे सो मैंने उस दिन प्रेमी धर्म का निर्वाह किया और पहली बार शराब पी. इसमें मेरे उन पियक्कड़ दोस्तों की भी भूमिका सहयोगात्मक रही जो मेरे पैसे से मुझे ही पिलाकर, और खुद पीकर मुझे सांत्वना देने के बहाने लुत्फ उठा रहे थे. मैं पहली बार पीकर न जाने क्या क्या बक रहा था. लेकिन पुष्पा मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था यह पक्का है. क्योंकि अगली सुबह भी दोस्तों की सुई नाम पर अटकी रही. यानी मैंने नशे में भी दोस्तों को सिर्फ कहानियां ही सुनाईं. मेरी और तुम्हारी कहानियां. वो कहानियां जो सिर्फ फिक्शन थीं और लोगों को सच लगती थीं.
मेरी शादी हो गई उसी लड़की से जिसे पापा ने मेरे लिए पसंद किया था. उसका नाम रागिनी था. मुझे यह नाम अच्छा लगा. यह वैसा ही नाम था जैसा मैं अपनी प्रेमिका का चाहता था. सच कहता हूं उस दिन मेरे मन से तुमसे बिछडऩे की तकलीफ थोड़ी कम हुई थी. रागिनी...कितना सुंदर नाम था. अब जब भी मैं कोई कहानी बुनता उसका साया तुम ही होतीं और नाम रागिनी यानी मेरी होने वाली पत्नी का. मेरी कहानियों के शेड्स चेंज हो रहे थे. उनकी चर्चा लगातार बढ़ रही थी. सच कहूं मेरी कहानियां तुमसे उपजीं थीं और तुम मेरे कल्पनालोक से. मुझे तुम्हारी आवाज याद आने लगी जब तुमने अपनी शादी से पहले वाली रात मेरे दोस्त के फोन पर बात की थी. बात क्या थी वो आंसुओं की बरसात थी. मैं दोनों हाथों से तुम्हारे आंखों से बहती बरसात सकेर रहा था.
जिस दिन मेरा विवाह हुआ मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोचता रहा. हालांकि शादी के कार्ड पर मनोज परिणय रागिनी मुझे मनोज परिणय पुष्पा से ज्यादा अच्छा लग रहा था.
रागिनी मेरी जिंदगी में मेरी पसंद से नहीं आई थी. वो पापा की पसंद थी. मुझे जाने क्यों लगता कि पापा जाते-जाते मुझसे मेरी उन सारी बातों का बदला ले गये हैं, जिन पर उन्होंने जिंदगी भर कुछ नहीं कहा. मैं रागिनी से बात करना पसंद नहीं करता था. तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन सच यही है कि सुहागरात वाले दिन मैं सारी रात खिड़की के पास खड़ा रहा. और सच्चे प्रेमी की भूमिका निभाता रहा. आसमान पर कोई चांद भी नहीं था देखने को. हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि मैं काफी नर्वस था. खुद को रागिनी के काबिल नहीं समझता था. वो इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी. इसका मतलब वो पढऩे में अच्छी रही होगी. मुझे पढऩे में अच्छे लोगों से एक किस्म की चिढ़ हो गई थी. उसका नाम भी मेरे नाम से अच्छा था. और वो बहुत खूबसूरत थी. लेकिन इससे क्या मैं तो तुम्हें प्यार करता था. तुम्हारी उस टूटी सी आवाज को जिसमें तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा. तुम्हें तो पता है कि हमारा समय कोई ईमेल और फेसबुक वाला तो था नहीं. मैंने तुम्हें हमेशा परछाइयों में देखा था और एकाध बार फोन पर सुना था. जिसमें आधे वक्त तुम रोती रहती थीं.
खूबसूरती एक किस्म का जादू होती है. रागिनी बहुत प्यारी निकली. जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही $जहीन. मैं उसके सामने हमेशा पिद्दी साबित होता. वैसे मैं हमेशा से दब्बू ही रहा था. रागिनी में पापा के जैसा अधिकार था. उसके सामने आते ही मैं अच्छे बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगता. धीरे-धीरे मैं तुम्हें भूलने लगा. या फिर याद करता तो यह सोचकर गर्व से भर जाता कि तुम्हारे काले गंजे पति के मुकाबले मुझे अच्छी बहुत अच्छी पत्नी मिली है. और बुरा मत मानना, कई बार मैंने यह भी सोचा कि अच्छा हुआ तुम मेरी पत्नी न हुईं. तुम्हारा सांवला रंग, औसत कद सब रागिनी के आगे बौने पड़ते और तुम्हें खोने का दुख सुख में बदलने लगता.
मां को अचार बनाने में मदद करने से लेकर मेरी कहानियों में जरूरी तब्दीलियां करने तक रागिनी समर्थ थी. थोड़े ही दिनों में मुझे रागिनी से चिढ़ होने लगी. वो मेरे होने को खा जाती थी. मैं खुद को पिटा हुआ सा मनोज महसूस करने लगा. जिसका नाम तक घिसा हुआ हो वो भला क्या करेगा. मेरी कहानियां भी अब पिटने लगी थीं. पत्रिकाओं से लौटी कहानियों को मैं छुपाकर रखने लगा. मैं तुम्हें फिर से याद करने लगा. एक दिन मैंने रागिनी से बदला लेने के लिए उसे तुम्हारे बारे में बता दिया. तुम यकीन नहीं करोगी उसने मेरा कैसा मजाक उड़ाया. कितना हंसी थी वो. उसने मां को भी इस बात के बारे में बताया. फिर मां और वो दोनों खूब देर तक हंसती रहीं. उस दिन मैं अंदर ही अंदर खूब रोया. मुझे जाने क्यों लगा कि तुम होतीं तो मुझे संभाल लेतीं. मैंने तुम्हारा नंबर भी उस दिन लगाया था लेकिन तुम्हारे पति की आवाज सुनकर रख दिया. उस रात मैंने उन सब लड़कियों को याद किया जिनके साथ मैंने कभी न कभी होना चाहा था.
मैंने रागिनी से अंदर ही अंदर हार मान ली थी. जैसे पापा से मान ली थी. एक चिढ़ी हुई हार. लेकिन तुम्हें पता है उस दिन जब मेरे बच्चे को जन्म देते हुए वो बिलख रही थी तो मेरे अंदर का राक्षस जाग उठा था. मुझे जीवन में पहली बार खुशी का अनुभव हो रहा था. सब समझ रहे थे कि बच्चे की आमद की खुशी है लेकिन मैं असल में रागिनी से अपना बदला पूरा होता महसूस कर रहा था. लेकिन रागिनी तो जैसे जीत लेकर ही पैदा हुई थी. बच्चा होने के बाद उसका यशगान और बढ़ गया. मेरी उसके प्रति चिढ़ का संबंध तुम्हारे प्रति प्रेम से नहीं रह गया था फिर भी मैं उन दोनों को आपस में मिलाता रहता था.
मेरी कहानियां मुझसे रूठकर जाने लगीं. मैं एक तिनके में समूची प्रकृति को उकेरने का माद्दा रखने वाला कोरे कागज के आगे निरीह महसूस करने लगा. मेरे सारे शब्द मुझसे रूठ गया. मुझे जब अपने बच्चे का नाम रखना था तब भी मैं कुछ नहीं सोच पाया और रागिनी ने उसका नाम प्रखर रख दिया. कितना सुंदर नाम. मैं अपने निरीह नाम के साथ वापस अपनी दुनिया में लौट आया.
तुम सोच रही होगी कि आज ये क्या मुसीबत हाथ लगी है. जिंदगी भर तो कुछ कहा नहीं और अब ये खर्रा लिख भेजा है. लेकिन पुष्पा ये बहुत जरूरी है. मैंं यह नहीं लिखूंगा तो मर जाऊंगा. तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो. यह मैं इतने यकीन से क्यों कह रहा हूं पता नहीं. हमें दुनिया के वही हिस्से सबसे बेहतरीन लगते हैं जहां हम गये नहीं होते. वही पल जिन्हें हमने जिया नहीं होता. शायद इसीलिए मेरी और तुम्हारी दुनिया ही सबसे बड़ा सच रही हमेशा मेरे लिए.
प्रखर बहुत शैतान है. वो मेरे सामने यूं खड़ा होता है जैसे पापा खड़े होते थे. वो मुझे यूं डांटता है, जैसे मैं उसका पिता नहीं वो मेरा पिता है. मां और रागिनी दोनों हंसती हैं. मैं खुद में लौट आता हूं. अंदर ही अंदर महसूस होता है कि मैं बोनसाई होता जा रहा हूं. मेरे अपने गढ़े हुए जीवन का आकार मुझसे बड़ा होता जा रहा है. पुष्पा अगर तुम होतीं तो ऐसा नहीं होता ना? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता, वो प्यार जो मैं रागिनी को उसके डर के चलते नहीं कर पाया. तुम मेरा आकाश, मेरी जमीन, मेरा स्वप्न, मेरा यथार्थ सब कुछ. इस रागिनी ने आकर मेरा सब कुछ छीन लिया. मुझे बोनसाई बनाकर रख दिया है. मैं अब अपना जीवन ढो नहीं पा रहा हूं. मेरी कहानियों ने मेरा हाथ छोड़ दिया है.
तुम्हें याद करते हुए मैं इस दुनिया से विदा ले रहा हूं. तुम अपना ख्याल रखना और याद रखना कि मैंने हमेशा तुम्हें बहुत प्यार किया.
तुम्हारा
मनोज...
इसके पहले कि मैं इस चिट्ठी को कहानी का नाम देता यह रागिनी के हाथ लग गई और उसका हंसते-हंसते बुरा हाल है. वो इसका पाठ करके मां को भी सुना चुकी है. मां अपनी हंसी का सुर रागिनी की हंसी से मिलाते हुए पूछती हैं कि तुम मसखरी करने से बाज नहीं आओगे? प्रखर चिट्ठी को हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहा है. रागिनी मुझे चिकोटी काटकर पूछती है ये पुष्पा कौन है? मैं हंसकर कहता हूं 'कोई नहीं'. शायद जिंदगी में पहली बार मेरे कानों ने अपने मुंह से कहा कोई सच सुना था...
(दैनिक जागरण के साहित्य विशेषांक पुनर्नवा में प्रकाशित)
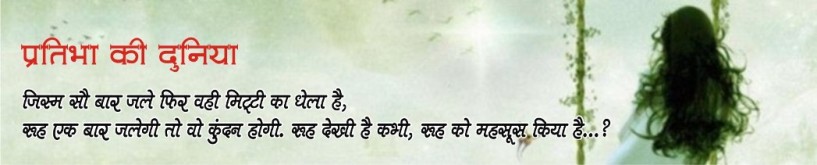






















.jpg)

